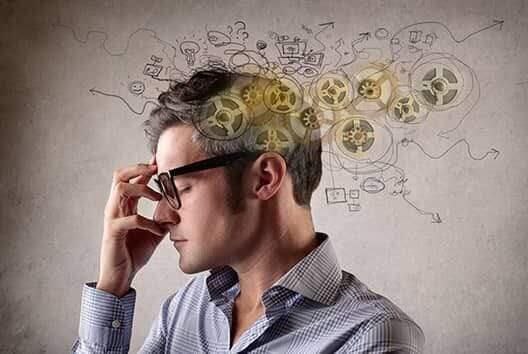“माइंड वांडरिंग” (Mind Wandering) एक अस्थिर मानसिक ध्यान की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति वर्तमान विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और उसके विचार अनजाने में अतीत, भविष्य या असंबंधित विषयों की ओर बह जाते हैं। यदि यह स्थिति पुरानी हो जाए और व्यक्ति के मानसिक विषय मुख्यतः नकारात्मक, पुनरावृत्तिमूलक और अनुपयोगी हों, तो मनोवैज्ञानिक इसे “मनमंथन” कहते हैं। डॉ. चिज़री इसे केवल व्यक्तिगत चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक उत्पादकता, पारिवारिक एकता और यहां तक कि स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक खतरा मानते हैं।
मनमंथन, जो क्षणिक विचारों या तटस्थ कल्पनाओं से भिन्न होता है, अक्सर अपराधबोध, अस्मिता की कमी, भविष्य की चिंता या कड़वे अतीत की समीक्षा के इर्द-गिर्द घूमता है। तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि मनमंथन के दौरान मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स (Prefrontal Cortex) और डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क (Default Mode Network) अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं; अर्थात् मस्तिष्क ऐसे पुनरावर्ती मानसिक कार्यों में उलझ जाता है जो परिणामहीन और चिंता से भरे होते हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा को समाप्त करती है, बल्कि प्रमुख अवसाद, व्यापक चिंता विकार, PTSD और OCD जैसे मूड विकारों से सीधे जुड़ी होती है।
चिज़री चेतावनी देते हैं कि यदि मनमंथन समय पर पहचाना और नियंत्रित न किया जाए, तो यह एक बुरे चक्र को जन्म दे सकता है: व्यक्ति विचारों के कारण अपनी एकाग्रता और कार्यकुशलता खो देता है; इस असफलता से उत्पन्न महसूस किया गया असमर्थता मनमंथन को पुनः पोषित करती है। यह चक्र बिना पेशेवर हस्तक्षेप के वर्षों तक जारी रह सकता है और इससे सामाजिक अलगाव, निद्रा विकार, निर्णय लेने में असमर्थता, प्रेरणा की कमी और यहां तक कि आत्म-हानि के विचार उत्पन्न हो सकते हैं।
डॉ. चिज़री आगे बताते हैं कि मनमंथन, यद्यपि एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, इसके बाहरी प्रभाव भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे कार्यस्थल में जो कर्मचारी लगातार मनमंथन में फंसे होते हैं, उन्हें अधिक बर्नआउट, लगातार गलतियाँ, लंबी अनुपस्थिति और कार्य संतोष में कमी होती है। शैक्षिक प्रणाली में भी, जो छात्र अपने मस्तिष्क को पिछले असफलताओं या भविष्य के भय में फंसा पाते हैं, वे प्रभावी रूप से सीख नहीं पाते। व्यापक स्तर पर, यह घटना मानव संसाधन की उत्पादकता को कम कर सकती है और स्वास्थ्य प्रणाली के मनोवैज्ञानिक खर्चों को बढ़ा सकती है।
समाजिक दृष्टिकोण से, चिज़री इसे तलाक की दरों में वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता में कमी और संस्थागत कार्यप्रणाली में विघटन से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि मनमंथन सार्वजनिक सहिष्णुता की सीमा घटाने और संगठनात्मक व पारिवारिक तनाव बढ़ाने वाले छुपे हुए कारणों में से एक है। साथ ही, नीति निर्धारक जो नकारात्मक मानसिक चक्र में फंसे होते हैं, वे राष्ट्रीय और सामूहिक हितों की व्यापक समझ प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए, इस मुद्दे पर ध्यान देना न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए, बल्कि बेहतर शासन के लिए भी आवश्यक है।
मनमंथन के प्रबंधन के उपाय तीन स्तरों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं: रोकथाम, मनोचिकित्सा हस्तक्षेप, और सामाजिक पुनर्वास। रोकथाम के स्तर पर, स्कूलों, मीडिया और कार्यस्थलों के माध्यम से माइंडफुलनेस, लचीलापन, तनाव प्रबंधन और भावनात्मक नियंत्रण कौशल की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिज़री मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूल और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल करने और व्यावसायिक संस्थाओं व मीडिया के सहयोग से जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हैं। वे स्कैंडिनेवियाई देशों के सफल कार्यक्रमों का उदाहरण देते हैं, जहां व्यापक शिक्षा ने किशोर पीढ़ी में मूड विकारों और आत्म-हानि की घटनाओं को उल्लेखनीय रूप से कम किया है।
हस्तक्षेप स्तर पर, वे विशेष रूप से संज्ञानात्मक-व्यवहार थेरेपी (CBT) का उल्लेख करते हैं, जो विनाशकारी सोच पैटर्न को सुधारकर मनमंथन के चक्र को तोड़ने में मदद करती है। साथ ही, स्वीकार्यता और प्रतिबद्धता आधारित थेरेपी (ACT) और डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी (DBT) भी विशिष्ट मामलों में प्रभावी हैं। गंभीर मामलों में, एंटीडिप्रेसेंट या एंटी-एंग्जायटी दवाओं का उपयोग सलाहकार मनोचिकित्सक की निगरानी में किया जाता है। वे जोर देते हैं कि उपचार केवल दवा तक सीमित नहीं है; रोगी की सक्रिय भागीदारी, जीवनशैली का पुनर्निर्माण, चिकित्सक के साथ प्रभावी संवाद, और दैनिक गतिविधियों में क्रमिक वापसी उपचार की सफलता के पूरक तत्व हैं।
चिज़री परिवार, मित्रों और देखभाल करने वालों की भूमिका को भी आवश्यक मानते हैं। उनका कहना है कि मनमंथन से पीड़ित व्यक्ति को सबसे अधिक सुनने, सहानुभूति और मानसिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वे सलाह देते हैं कि आस-पास के लोग सामान्य समाधान देने या आलोचना करने के बजाय सक्रिय सुनवाई का अभ्यास करें। दवाओं की याद दिलाना, चिकित्सा सत्रों में साथ जाना, नियमित नींद और व्यायाम जैसे स्वस्थ आदतें अपनाने में मदद करना, और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना उपचार प्रक्रिया को तेज कर सकता है।
अंत में, चिज़री संस्थागत रूप से मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा पर गहरी आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि जैसे चिकित्सा उपकरणों को महत्व दिया जाता है, वैसे ही समाज के “मानसिक उपकरणों” का भी समर्थन होना चाहिए। इसका मतलब है कि मनोचिकित्सा सेवाओं के लिए बजट आवंटन, परामर्श सत्रों के लिए बीमा कवरेज, स्थानीय केंद्रों में मनोवैज्ञानिकों का प्रशिक्षण, और मानसिक मुद्दों पर सार्वजनिक संवाद के लिए मीडिया समर्थन, ईरानी स्वास्थ्य प्रणाली की प्राथमिकताएँ होनी चाहिए।
वे चेतावनी देते हैं कि एक ऐसी दुनिया में जहां डिजिटल अकेलापन, आर्थिक असुरक्षा, और मानसिक थकावट दिन-ब-दिन बढ़ रही है, विशेषज्ञ संस्थान, मीडिया, पेशेवर संघ और नीति निर्माता मनमंथन पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें एक ऐसी पीढ़ी मिलेगी जो बाहर से स्वस्थ लगेगी, पर अंदर से थकी हुई और निरुत्साहित होगी।
डॉ. चिज़री अंत में मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं, और सुझाव देते हैं कि तेहरान प्रांत की मेडिकल और फार्मास्यूटिकल उपकरण संघ मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलकर जागरूकता अभियानों का आयोजन करे, रोगियों और परिवारों के लिए शैक्षिक पुस्तिकाएँ तैयार करे, और पिछड़े इलाकों में परामर्श क्लीनिक स्थापित करे; यह कदम देश में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच नए प्रकार के समन्वय मॉडल को प्रस्तुत कर सकता है। उनका मानना है कि यह स्वास्थ्य से जुड़े हर पेशे का नैतिक दायित्व है।
इस लेख में डॉ. अलिरज़ा चिज़री न केवल एक पेशेवर कार्यकर्ता के रूप में, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की आवाज़ के रूप में, एक मौन लेकिन गहरे और व्यापक प्रभाव वाले fenômenon की ओर समाज, मीडिया और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। थका हुआ मन बीमार शरीर को जन्म देता है; और एक समाज जिसकी मानसिकता मनमंथन में फंसी हो, वह विकास, समृद्धि और न्याय के मार्ग पर मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकता।